Atalaantis Dveep Ka Rahasy | अटलांटिस द्वीप का रहस्य | अटलांटिस द्वीप का अनसुलझे रहस्य
अटलांटिस द्वीप - विश्व-प्रसिद्ध अनसुलझे रहस्य
क्या कभी अटलांटिक महासागर के मध्य में एक विशाल और विकसित सभ्यता फली फूली थी?
यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा किए गए वर्णन से ऐसा लगता है कि अटलांटिस की सभ्यता उस युग की एक सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली व्यवस्था थी, जिसकी स्वर्ग से तुलना करना अतिशयोक्ति न होगी।
तभी अचानक एक ज्वालामुखी फटा।
ऐसा लगा कि जैसे आसमान से मौत की बारिश हुई हो और अटलांटिस द्वीप महासागर की गहराइयों में विलीन हो
गया।
आखिरकार अटलांटिसवासियों को किस अपराध की सजा भुगतनी पड़ी थी? क्या यूनान में पुरातात्विक खुदाई में निकला शहर आक्रोतिरी ही अटलांटिस का खोया हुआ शहर है? क्या प्लेटो द्वारा किया गया वर्णन सिर्फ एक कहानी ही है?
इन्हीं रहस्यों के ताने-बाने में लिपटा है इस लुप्त सभ्यता का खोया हुआ अस्तित्व। दुनिया भर के भूगर्भशास्त्री ज्वालामुखी विशेषज्ञ तथा पुरातत्वशास्त्री निरंतर इस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए प्रयत्नशील हैं।
साढ़े तीन हजार साल पहले की एक शाम।
अटलांटिस द्वीप पर बसा हुआ नगर हमेशा की तरह दिन भर का काम-काज समाप्त करके रात बिताने की तैयारियां कर रहा था। नगर की पतली गलियां हंसते और आपस में बाते करते नागरिकों से भरने लगी थीं। औरतें अपने घरों के दरवाजों पर बैठी गप्पें मार रही थीं। वातावरण शांत था और मौसम का मिजाज भी अनुकूल ही था। अचानक पूरे नगर को एक विचित्र तरह की गर्मी ने अपनी लपेट में ले लिया।
द्वीप के आस-पास का समुद्र सीसे के रंग का हो गया और धरती की गहराइयों से थरथराहट की दबी-दबी आवाजें आने लगीं। पहले ये आवाजें रुक-रुक कर आईं फिर लगातार सुनाई देने लगीं। द्वीप निवासी घबरा गए। उन्हें डर था कि उनके द्वीप का 5000 फुट ऊंचा ज्वालामुखी फट पड़ने को है।
उन्हें लगा कि धरती हिला देने वाली ताकतों का मालिक उनका देवता लम्बी निद्रा से जागने वाला है।
इतना समझने के बाद भी अटलांटिस द्वीप के वासी यह नहीं समझ पाए कि पृथ्वी के गर्भ से आने वाली ये आवाजें उनके द्वीप, उनके नगर और उनकी समूची सभ्यता के विनाश की आहटें हैं। यही हुआ। पहले दम घोंट देने वाला गहरा धुआं उठा, फिर सुलगते हुए पत्थरों की वर्षा हुई और इसके बाद चारों तरफ आग उड़ने लगी। ज्वालामुखी का गर्भ अचानक दबाव से फट गया। वह लाखों टन की ठोस चट्टानों
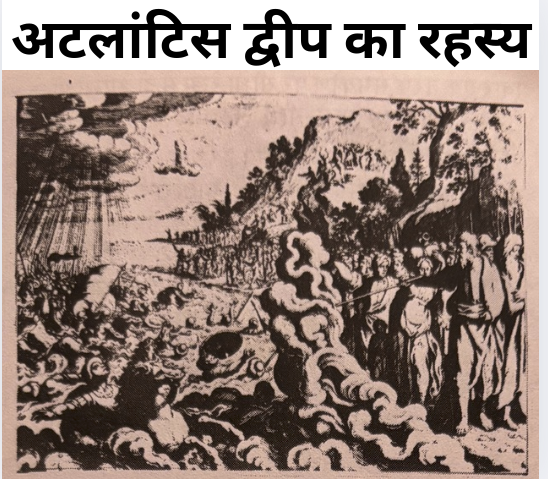
की वर्षा करता हुआ अपनी ही जगह पर धंस गया, जिसकी वजह से एक 37 मील लम्बा-चौडा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को भरने के लिए समुद्र की लहरें चारों ओर से टट पड़ी।
आज के वैज्ञानिकों व ज्वालामुखी विशेषज्ञों का अनुमान है कि 500 से 1000 परमाणु बमों की ताकत के बराबर विस्फोट क्षमता से वह ज्वालमुखी फटा होगा। काली राख की वर्षा के कारण उस समुद्र के आकाश पर कई सप्ताह तक रात जैसा अंधेरा बना रहा। उस राख के अवशेष आज भी बचे-खचे द्वीप पर देखे जा सकते नाम दिया था। हैं। इस बचे हुए द्वीप को प्राचीन समय में यूनानियों ने कैलिस्टे (Kelliste) का
अटलांटिस द्वीप के ऐतिहासिकता का केवल एक ही सर्वमान्य प्रमाण उपलब्ध है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपने शिष्यों के साथ बातचीत में इस द्वीप, उसकी सभ्यता व उसके विनाश के कारणों का विस्तृत उल्लेख किया है।
प्लेटो के अनुसार अटलांटिस का नगर तरह-तरह की कीमती वस्तुओं, विभिन्न प्रकार के जानवरों और मवेशियों, तांबे की मिश्र धातु व अन्य खनिज पदार्थों से भरा-पूरा था। पूरा शहर 5 खण्डों में बंटा हुआ था, जो वृत्ताकार रूप से व्यवस्थित थे। इसके विभिन्न बंदरगाह नहरों द्वारा जुड़े हुए थे। शहर के बीच में एक विशाल महल व मंदिर था। इन दोनों के शीर्ष सोने व चांदी से मढ़े हुए थे। सोने के बने हुए सात पंखदार घोड़ों के रथ पर सवार इस शहर का देवता पोसीडोन मंदिर में स्थापित था। भूकम्प के इस देवता की पूरे नगर में पूजा की जाती थी।
प्लेटो के वर्णन में आगे बताया गया है कि हर विकसित सभ्यता की तरह अटलांटिस के पतन के दिन भी आए और वहां के निवासी साम्राज्य, शक्ति और धन-धान्य की पूजा करने लगे। अटलांटिस की फौजें आक्रमण और युद्ध के अभियान पर निकल पड़ीं। उन्होंने भूमध्य सागर की तटवर्ती बस्तियों के निवासियों को अपना गुलाम बना लिया लेकिन एथेंसवासियों के सामने उनकी एक न चली। एथेंस की फौज ने
अटलांटिस की फौजों को हरा कर भगा दिया परंत अटलांटिस के नैतिक पतन का दण्ड अभी अधूरा था। इसके बाद भीषण भूकम्पों और बाढ़ों ने एक ही रात में अटलांटिस को अपने आगोश में लेकर तबाह कर दिया।
प्लेटो के अनुसार 12 हजार साल पहले जिब्राल्टर के जलडमरूमध्य के आस-पास अटलांटिस का अस्तित्व था। यहीं से शुरू होती है अटलांटिस की लुप्त सभ्यता के रहस्य की कहानी। प्लेटो की बातचीत में अटलांटिस की कहानी मुख्य रूप से उनके भतीजे क्रिटियास (Critias) द्वारा सुनाई गई थी, जिसके बारे में स्वयं प्लेटो के गुरू सकरात ने कहा था "यह एक तथ्य है न कि केवल कहानी"।
क्रिटियास का यह भी दावा था कि उसने यह कहानी अपने परबाबा ड्रोपिडस (Dropides) से सुनी थी और ड्रोपिडस ने इसे यूनानी इतिहास में अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध सोलन (Solan) से सुना था। सोलन को सबसे विख्यात विधि-निर्माता तथा यूनान के सात महान् संतों में सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता था। सोलन 640 ईसा पूर्व से लेकर 558 ईसा पूर्व तक जीवित रहा। इसके दो सौ वर्ष बाद प्लेटो ने यह कहानी लिखी।
सोलन का कहना था कि उसने यह कहानी ईसा से 590 वर्ष पूर्व मिस्र के एक पुजारी से सुनी थी। सोलन ने इस महान् कहानी से प्रभावित होकर इसका अनुवाद यूनानी भाषा की कविता में कर डाला। इससे लगता है कि यूनानियों से पहले मिस्रियों को भी अटलांटिस के अस्तित्व का ज्ञान था।
प्लेटो द्वारा किया गया वर्णन ऐतिहासिक कम दार्शनिक अधिक है।
वह एथेंस के वैभव और गरिमा से अधिक प्रभावित जान पड़ता है। अटलांटिस का अस्तित्व उस समय और भी रहस्यपूर्ण हो गया जब प्लेटो के शिष्य अरस्तु (Aristotle) ने इसे मात्र काव्यात्मक कथा ही माना परंतु ईसा से 300 वर्ष पूर्व प्लेटो के प्रथम व्याख्याता क्रेण्टर (Crantor) ने अटलांटिस के वर्णन को तथ्यात्मक करार दिया। कहा जाता है कि क्रेण्टर के कुछ शताब्दी बाद दार्शनिक पोसीडोनियस (Posidonius) (135-50 ईसा पूर्व) ने प्लेटो के वर्णन को केवल एक कथा मात्र मानने से इंकार कर दिया।
इस तरह पूरी 23 शताब्दियों से आज तक अटलांटिस का रहस्य इसी तरह के विवादों में घिरा रहा है। अटलांटिस के बारे में धार्मिक पुजारियों, काले जाद के विशेषज्ञों तथा अफवाहबाजों ने तरह-तरह की कहानियां गढ़ लीं। किसी ने कहा कि अटलांटिस के पेड़ों में सोने के फल लगते थे तो किसी ने कहा कि वहां की नहरों से दूध और शहद बहता था।
प्लेटो को विश्वास था अटलांटिस (Atlantis) द्वीप अटलांटिक (Atlantic) के बीच में ही था। प्लेटो का समर्थन करने वाले आधुनिक विद्वानों का मत है कि अजोरस (Azores) केप वेर्डे आइलैण्ड (Cape Verde Islands) केनरीज (Canaries) तथा मेडीरा (Madeira) की चोटियां अटलांटिस द्वीप की ही थीं. जो एशिया और अफ्रीका के संयुक्त क्षेत्रफल से भी बड़ा था।
15वीं शताब्दी के यूरोपीय अन्वेषकों ने कल्पना के आधार पर ही अटलांटिस को अपने नक्शों में शामिल कर लिया।
हर नई खोज को अटलांटिस के रूप में देखने की आदत बन गई।
अमेरिका की खोज होते ही कुछ समय के लिए मान लिया गया कि अटलांटिस की खोज हो गई है।
अटलांटिस में लोगों की दिलचस्पी इतनी बड़ी कि 19वीं शताब्दी तक अटलांटोलोजी (Atlantology) नामक विज्ञान की शाखा की स्थापना के दावे किए जाने लगे।
इस विज्ञान के सबसे प्रमुख अध्येता थे इग्नेशियस डोनेली (Ignatius Donnelly) नामक अमेरिकी राजनीतिज्ञ जो अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य भी थे।
सन् 1882 में डोनेली ने अंटलाटिस द एण्टेडिल्यूवियन वर्ल्ड (Atlantis: The Antediluvian World) नामक पुस्तक लिखी जो रातों-रात 'बेस्ट-सैलर' बन गई।
डोनेली ने अपना सिद्धांत अमेरिका की कोलम्बस पूर्व सभ्यता तथा प्राचीन मिस्र संस्कृति के बीच कुछ समानताओं के आधार पर गढ़ा।
पिरामिडों के निर्माण, ममी बनाने के कला, 365 दिन के कलैण्डर तथा बाढ़ों की परम्परा को देखते हुए डोनेली ने साबित किया कि उक्त दोनों सभ्यताएं अटलांटिस की ही देन थी। अटलांटिस के नष्ट हो जाने के बाद उसके पूर्व और पश्चिम में अलग-अलग सभ्यताओं ने जन्म ले लिया। डोनेली ने अपनी सामग्री पुरातत्व, मिथक, भाषा भूविज्ञान, जंतु व जीव विज्ञान से प्राप्त की। अपने आप को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए डोनेली ने इन विज्ञानों से तर्क लेकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रयोग करके उक्त सिद्धांत का ताना-बाना बुन दिया।
आज भी डोनेली के बहुत से समर्थक मौजूद हैं।
परंतु डोनेली के सिद्धात का यह केन्द्रीय विश्वास कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर के बीच में था, ठुकरा दिया गया है। आधुनिक सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाताओं ने जांच करके पता लगाया है कि 3 करोड़ 60 लाख वर्ग मील की अटलांटिक महासागर की सतह पर अटलांटिस में आए वर्णित भूकम्प का कोई चिह्न नहीं मिलता। 12,500 मील लम्बी एक ज्वालामुखी पर्वत माला अवश्य महासागर में डूबी हुई है लेकिन जहां यह पर्वत माला समुद्र से निकलती है, वहां अटलांटिस के डूबने की जगह बताई जाती है।
सन् 1912 में अमेरिका की एक सनसनीखेज पत्रकारिता ने अटलांटिस की कथा को पुनः नया जीवन प्रदान किया। 20 अक्तूबर को विलियन रुडोल्फ हर्स्ट (Villian Rudolph Hearst) ने 'न्यूयॉर्क अमेरिकन' नामक अपने पत्र में एक मोटा शीर्षक प्रकाशित किया- 'सभी सभ्यताओं के स्रोत अटलांटिस को मैंने कैसे खोजा?' (How I found the lost Atlantis the source of all civilizations)।
इस खोज के लेखक का नाम था डा. पाल श्लीमान (Dr. Paul Schliemann) जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे ट्रॉय के एक अन्वेषक के पोते हैं। डा. पाल का कहना था कि उनके बाबा ने ट्रॉय की खोज के दौरान तांबे का
बाइबिल की कहानी पर आधारित चित्र : हजरत मूसा को रास्ता देने वाले
लाल सागर ने फराओ की सेना को नष्ट कर दिया।
एक विशाल घड़ा प्राप्त किया था, जिस पर खुदा था : 'अटलांटिस के राजा क्रोनोस की ओर से उपहार'।
इसके अलावा भी डा. पाल ने कई दावे किए लेकिन यह कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्र एक सनसनी पैदा करके रह गई। सन् 1921 में रसायन शास्त्र में नोबल पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेज वैज्ञानिक फ्रेड्रिक सोडी (Fredrick Soddy) ने अटलांटिस के रहस्य को खोजने की असफल कोशिश की।
एक जर्मन पुरातत्वीय पत्रकार सी. डब्ल्यू. सेराम (C. W. Ceram) ने हाल ही में इस विषय पर 20,000 ग्रंथ लिखे जाने का आंकड़ा पेश किया है।
एक अमेरिकन अतींद्रियदर्शी (Clairvoyant) तथा फोटोग्राफर एडगर सायके (Edgar Cayce) (1877-1945) ने 1923 से 1944 के बीच तमाम लोगों को हिप्नोटाइज करके अतींद्रिय दृष्टि से अटलांटिस सभ्यता के चित्र प्राप्त किए, जो प्लेटो के वर्णनों से मिलते-जुलते थे।
यद्यपि सायके ने प्लेटो के वर्णन को नहीं पढ़ा था।
सायके के अनुसार अटलांटिसवासियों ने अणुशक्ति को अपने वश में कर लिया था, जो ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व विस्फोट का शिकार हो गई।
सायके का इशारा था कि वर्तमान सं.रा. अमेरिका ही अटलांटिस है क्योंकि वह मैक्सिको की खाड़ी तथा जिब्राल्टर के जलडमरूमध्य के बीच स्थित था।
सन् 1968 में बहामा में डा. मेंसन वेलेंटाइन (Dr. Manson Valentine) ने बहामा के जल की गहराइयों में गोता लगा कर कई मील तक फैली हुई विचित्र संरचनाएं देखीं।
सन् 1968 में उन्होंने ही नार्थ बिमिनी (North Bimini) के छोटे से द्वीप के पानी में कई सौ गज लम्बी दैत्याकार दीबार देखी।
16 वर्ग फुट के पत्थरों
से बनी यह दीवार एक तरफ समकोण पर सीधी रेखा में दो शाखाओं के रूप में बनी हुई थी।
इस दीवार का संबंध सीधे-सीधे अटलांटिस से जोड़ दिया गया।
सन् 1967 में प्रमुख पुरातत्वशास्त्री स्पाइरिडोन मैरिनाटोस (Spyridon Marinatos) ने कैलिस्टे द्वीप के नीचे दबे सांतोरीनी (Santorini) नामक प्राचीन नगर की खुदाई शुरू की।
इससे 2 साल पहले अमेरिकी वैज्ञानिक द्रागोस्लाव निन्कोविच (Dragoslav Ninkovich) तथा बी. सी. हीजेन (B. C. Heezen) ने सांतोरीनी पर आए 3,500 वर्ष पुराने भूकम्प की जानकारी दी और उसकी तुलना सन् 1883 के अगस्त में जावा व सुमात्रा में फटने वाले क्राकाटोआ ज्वालामुखी से की।
सांतोरीनी पर फटे ज्वालामुखी ने क्राकाटोआ से 4 गुना अधिक विनाश किया था।
इस द्वीप की खुदाई में जले हुए दांत तथा कुछ हड्डियां मिली हैं।
सांतारीनी के अलावा समुद्रों के नीचे दबी हुई सभ्यताओं तथा भूखण्डों के नीचे छिपे हुए नगरों का अस्तित्व भी पुरातत्वशास्त्र के विकास के साथ उभरता जा रहा है।
इनके साथ अटलांटिस की कहानी में जरा भी समानता होने पर तुरंत दोनों का संबंध जोड़ दिया जाता है।
भारत के दो महान् महाकाव्यों 'रामायण' तथा 'महाभारत' में भी इस तरह के वर्णन हैं, जो अटलांटिस से मिलते-जुलते हैं। लगता है कि वैज्ञानिक संभवतः सांतोरीनी के खण्डहरों को ही अटलांटिस के साथ अंतिम रूप से जोड़ देंगे।
फिलहाल अटलांटिस की खोज जारी है।
वह आज भी विश्व के अंतिम अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है।